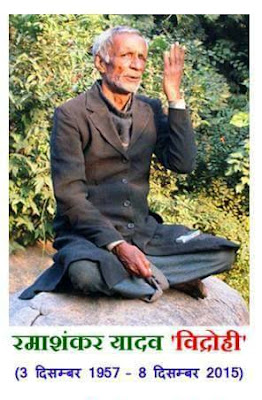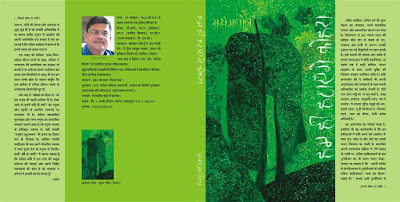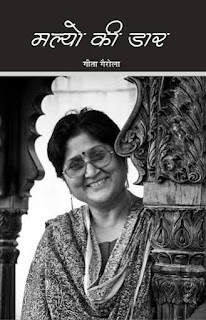परिवर्तन की गहरी उम्मीद से भरा हुआ कवि
हर बड़े कवि में ऐसी कुछ खासियतें होती हैं, जो उस कवि को अन्य से अलगाती हैं। उसका एक चेहरा बनाती हैं। यही खासियतें होती हैं, जो पाठकों को उस कवि से जोड़ती हैं। वैसे पाठक की पसंद और नापसंद, उसकी अपनी रुचि ,दृष्टि ,समझ और सरोकारों पर भी निर्भर करती है। फिर भी कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो हर पाठक को कवि की ओर आकर्शित करती हैं। वीरेन डंगवाल की कविताएं मैं लम्बे समय से पढ़ता आ रहा हूँ। ‘रामसिंह’ कविता से इस कवि से मेरा पहला-पहला परिचय हुआ,उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा। इस कवि के यहाँ मौजूद भाषा-षिल्प और संवेदना की विविधता ने इस क्रम को कभी टूटने नहीं दिया। जितना अधिक पढ़ता गया उतनी अधिक जीवन की परतें खुलती गई। हर बार कुछ नया मिला। यदि कोई पूछे कि मुझे वीरेन डंगवाल की कविता क्यों पसंद है?कुछ शब्दों या वाक्यों में मेरे लिए कह पाना मुश्किल है।
वीरेन डंगवाल की कविताओं में हमारे चारों ओर फैले गहरे अँधेरे और कालेपन के बीच जो उजाले की चमक तथा जीवन का सौंदर्य है,वह मुझे बहुत पसंद है। वह हमारे समय और समाज में व्याप्त भयावह कालेपन को दिखाते हुए हमें उसी के बीच नहीं छोड़कर आते हैं, बल्कि उससे बाहर निकाल कर लाते हैं। वह अपनी कविताओं में जहाँ बार-बार कहते हैं कि ‘बहुत कठिन समय है साथी’, वहीं बार-बार हमें जयघोष करती उन्मत्त भीड़ के चेहरों को भी दिखाते हैं। वह कभी नहीं कहते हैं कि इस ‘कठिन समय’ से निकलना कठिन है। उनकी कविताओं को पढ़कर अवसाद और निराशा की गर्त में पड़ा पाठक भी एक नए उजास से भर उठता है। उसे अँधेरे और कालेपन से लड़ते हुए लोग दिखाई देने लगते हैं। इस बात से उसका विश्वास बढ़ता है कि ‘कितनी भी बड़ी हो तोप/एक दिन तो होना ही है उसका मुँह बंद।’ वीरेन दा जांगर करते,खटते पिटते,लड़ते-भिड़ते, अनवरत सताए जाते,संतप्त-हृदय-पीडि़त,प्रच्छन्न क्रोध ,निस्सीम प्रेम और विस्तीर्ण त्याग से भरे जन के भीतर लपक रही खामोश आग को देख लेने वाले कवि हैं। इसी आग के बल पर तो ‘उजले दिन जरूर आयेंगे’ जैसा विश्वास उनके मन में हमेशा बना रहता है। वह कह पाते हैं-‘मैं नहीं तसल्ली झूठ-मूठ की देता हूँ/हर सपने के पीछे सच्चाई होती है/हर दौर कभी तो खत्म हुआ ही करता है/हर कठिनाई कुछ राह दिखा ही देती है।’ इस तसल्ली देने के पीछे उनके पास ठोस कारण हैं। उन्हें पता है कि-हैं अभी वे लोग जो ये बूझते हैं/विश्व के हित न्याय है अनमोल/ वही शिवि की तरह खुद को जांचते/ देते स्वयं को कबूतर के साथ ही में तोल। ’ वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि समाज में भले बेइमानी, अपराध,रिश्वतखोरी, झूठ,ठगी आदि कुप्रवृतियां बढ़ी हैं- ‘भाई भाई की गर्दन पर/ छूरी फेर रहा है/दोस्त मुकदमा लिखा रहे हैं/एक दूसरे पर/सौदा लेकर लौटती/स्त्री के गले से चेन तोड़/भागा जा रहा एक शोहदा/विधान भवन की तरफ।’ निर्दोष-सज्जन,भोले-भाले सरेआम चौराहे में मारे जा रहे हैं, हत्या को भी कला में बदल दिया जा रहा है तो हम भी इन्हें मान्यता देने लगें, यह मानने लग जाएं कि सबकुछ गड़बड़ है, हत्या एक कला है, अपराध एक हुनर और दुनिया का सारतत्व यही है, यह हरगिज नहीं हो सकता है-बेईमान सजे-बजे हैं/तो क्या हम मान लें कि/बेईमानी भी एक सजावट है?/ कातिल मजे में हैं/तो क्या हम मान लें कि कत्ल करना मजेदार काम है? कवि दृढ़ता से खुद ही अपने द्वारा उठाए प्रश्नों का उत्तर देता है कि-मसला मनुष्य का है/इसलिए हम तो हरगिज नहीं मानेंगे /कि मसले जाने के लिए ही/ बना है मनुष्य। वीरेन दा जीवन भर मनुष्य के मसले जाने के खिलाफ खड़े रहे। बूटों की ठक-ठक की ध्वनि उन्हें कभी भी पसंद नहीं आई। उनको पक्का यकीन है कि-‘इन्हीं सड़कों से चलकर/आते रहे हैं आतताई /इन्हीं पर चलकर आएंगे/हमारे भी जन। ’ भले ही अत्याचारियों ने शोषण-उत्पीड़न और अत्याचार के सभी साधन जुटा लिए हों और अभी हम नींद में हैं, ‘मगर जीवन हठीला फिर भी/बढ़ता ही जाता आगे/हमारी नींद के बावजूद।’ ‘....रात है रात बहुत रात बड़ी दूर तलक/सुबह होने में अभी देर हैं माना काफी/ पर न ये नींद रहे नींद फकत नींद नहीं/ये बने ख्वाब की तफसील अंधेरों की शिकस्त।’
वीरेन दा ‘इस मलिन समय’ में उस हर चीज की महिमा के गीत गाते हैं जो उम्मीद दिलाने वाली है और उस हर चीज पर चोट करते हैं, जो हमें गुलाम बनाती है, मनुष्य की आत्मा को रौंद डालती है तथा जीवन की महिमा को नष्ट करती है। वह सामंतवाद और पूंजीवाद दोनों पर एक साथ और सामूहिक रूप से हमला करने की बात करते हैं-कितना सताया तुम्हें-हमें/इन पोथियों-पोथियारों,ताकतवालों ने/इनका नाश हो/चलो मिलकर करते हैं इन पर घटाटोप/देखो तो चबा रहे हैं ये हमारे पहाड़ों को/गुड़ की भेली की तरह/खा रहे सब हमारे जंगल/हमारी भरी-पूरी नदियों को पी जा रहे हैं/पर इनकी भूख-प्यास मिटती नहीं/असली भूत-प्रेम-मसाण-राक्षस तो यही हुए/इनका नाश हो/इनका नाश करने के लिए चलो जुटते हैं /सभी एक साथ/करने से सब होगा भाई। ‘ करने से सब होता है’,का यकीन ही है जो हमें समय-सभ्यता के इस मोड़ तक लाया है और आगे भी ले जाएगा। इसी यकीन के साथ मनुष्यता जिंदा है और रहेगी, जीवन का सौंदर्य बना रहेगा, अंधकार खत्म होगा,आतंक सरीखी बिछी हुई बर्फ पिघलेगी,जीवनाकाश में छाए मेघ छिन्न-भिन्न हो पाएंगे। यह यकीन ही वीरेन दा की कविताओं की मूल संवेदना है और यही सबसे बड़ी सार्थकता व खूबसूरती भी।
हम जिस भयानक समय में रह रहे हैं वीरेन दा उसकी सच्चाई को बहुत गहराई से समझते-जानते हैं और उसका प्रतिसंसार रचते हैं। उस संसार का जो इस भयानक यथार्थ से लड़कर रचा जा सकता है। वह तेजी से बदलते संसार को तो अपनी कविताओं में दर्ज करते ही हैं साथ ही उससे बाहर निकलने वाले रास्ते की ओर भी संकेत करते हैं-‘जरा रगड़ो तो अपनी लोहे की कुल्हाड़ी की धार/पत्थर पर /उसे चिंगारियाँ फेंकते देखो/और इस विराट जंगल को कुत्ते की तरह/कांपते-किकियाते दुम दबाते।’ एक जनप्रतिबद्ध कवि जनता के पक्ष में खड़ा होकर केवल अन्धकार की सत्ता की ओर संकेत ही नहीं करता है, बल्कि वह जनता को सजग भी करता है। उसे अपने समय और समाज की असलियत को समझने व उसको बदलने के लिए प्रेरित भी करता है। अपनी समझ को और अधिक पुख्ता करने और बदलने को कहता है। वह जनता से कठमुल्लापन छोड़ने और संस्कृति के नाम पर कठमुल्लापन फैलाने वाली ताकतों के प्रति एक सही राह लेने और उनकी मुस्काती शक्लों में न फंसने की अपील करता है, क्योंकि वह जानता है कि ये ताकतें मनुष्यता की दुश्मन हैं। मनुष्यता ही है जो इस जीवन-जगत के सौन्दर्य को बचाकर रख सकेगी। वीरेन डंगवाल की ये काव्य पंक्तियाँ उसी सौन्दर्य को बचाने के पक्ष में एक विनम्र अपील है,जो आज के माहौल में और अधिक प्रासंगिक हो उठी हैं-ऐसे कठमुल्ले मत बनना/ बात नहीं हो मन की तो बस तन जाना /.............पोथी -पतरा-ज्ञान-कपट से बहुत बड़ा है मानव/ कठमुल्लापन छोड़ो,उस पर भी तो तनिक विचारो/काफी बुरा समय है साथी/गरज रहे हैं घन घमंड के नभ की फटती है छाती/अन्धकार की सत्ता चिलबिल -चिलबिल मानव-जीवन/जिस पर बिजली रह-रह अपना चाबुक चमकाती/संस्कृति के दर्पण में ये जो शक्लें हैं मुस्काती/इनकी/असल समझना साथी/अपनी समझ बदलना साथी (इतने भले नहीं बन जाना साथी) ‘ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ के नाम पर आज जिस तरह भारत की बहुलतावादी संस्कृति और समाज को नष्ट कर,उसे एक खास रंग में रंगने की जो कुत्सित और मानवता विरोधी चाल चली जा रही है, उसकी असलियत को समझने के लिए ये पंक्तियां प्रेरित करती हैं।
वीरेन डंगवाल जिस तरह से साधारण से साधारण व्यक्ति,जीव-जंतु,वस्तु या घटना को अपनी कविता में असाधारण या विशिष्ट बना देते हैं,वह अद्भुत है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि यह भी कविता का विषय हो सकता है, वह उस पर कविता लिख डालते हैं। उनके पास ऐसी कविताओं की एक पूरी श्रृंखला है, जो नगण्य माने जाने वाले विषयों पर लिखी गई हैं, जिनमें जीवन की छोटी-छोटी चीजों में छुपी भव्यता और विराट सौंदर्य के दर्शन होते हैं। आश्चर्य होता है ऐसी कवि-दृष्टि को देखकर जो ‘सर्दी में उबले आलू’ के दिल में भी पैठ जाती है,जो भीगे लाल कपड़े पे तहाके रखे पान के पत्तों में भारतीय उपमहाद्वीपता देख लेती है, जो कभी कढ़ाई में सनसनाते समोसे में अटक जाती है तो कभी स्याही की दवात में जा गिरी मक्खी पर। गाय,बिल्ली,सूअर,ऊँट,बंदर,चूहा,हाथी जैसे जानवरों को अपनी कविता में ले आते हैं। बिल्ली में शराफ़त और सूअर में सुंदरता देख लेता है। ‘पोस्टकार्ड-महिमा’ गाता है। इत्रों की ख़ुश्बू के बरक्स पोदीने की ख़ुश्बू को रख देता है। कवि होने का मतलब क्या होता है,वह इन ‘नगण्यता का गुणगान’ करती कविताओं को पढ़ते हुए समझा जा सकता है। कोई किताबी कवि ऐसी कविताएं हरगिज नहीं रच सकता है। यथार्थ और कल्पना का सही संतुलन कविता में किस तरह साधा जा सकता है? इन कविताओं से सीखा जा सकता है। उनका मानना है कि कविता लिखना खुद को प्यार करना है और खुद को बचाए रखना, इस तरह के विषयों पर कविता लिखना उसी दिषा में एक विनम्र प्रयास माना जा सकता है। दरअसल इस तरह के साधारण से साधारण विषयों पर कविता लिखना केवल कविता का मसला नहीं है बल्कि प्रकारांतर से हाशिए के जीवन को महत्व देना और उसके पक्ष में खड़े होना है। जब वीरेन दा कविता में इन साधारण सी चीजों के बारे में बात करते हैं तो कहीं न कहीं यह हाशिए के जीवन को केंद्र में लाने और अभिजात्य के खिलाफ लोक को खड़ा करने की कोशिश है। ऐसा वही कवि कर सकता है जो लोकजीवन के निकट हो तथा उससे उसकी गहरी संबंद्धता हो। वसंत के उरूज में ‘फ्यूंली’ जैसे उपेक्षित फूल को ऐसा कवि ही देख सकता है। वही श्रमजीवियों के जीवन-संघर्ष के साथ-साथ उनकी कमजोरियों और ताकत दोनों को अच्छी तरह पहचान सकता है। उनके लोकज्ञान को महत्व देता है। वह उनके भुजबल की ही नहीं अक्ल का भी प्रशंसक होता है। वीरेन डंगवाल ‘मल्लाह’ कविता में कहते हैं-‘सूंघ हवा को/बतला सकते हैं बरसेगा कब पानी/पैनी दृष्टि थाह लेती है पलक झपकते/डगमग लहरों के नीचे सारी गहराई’। कवि दुःख व्यक्त करता है कि शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होने के बावजूद उनकी पारिवारिक-सामाजिक-आर्थिक हालत बहुत कमजोर है। उनके पास न अच्छा खाने को है,न अच्छा पहनने को और न रहने को। इतना ही नहीं वे आपसी कलह, अशिक्षा, नशाखोरी, अपराध आदि के शिकार हैं। ठहरे पानी की तरह है इनका जीवन जिसमें सच्चे हुलास की एक लहर भी नहीं दिखाई देती है। कवि की सदइच्छा व्यक्त करता है-‘धनी बात के यों होते मेहनत के पक्के/कोई ले जाता इन तक भी सत जीवन का/दुनिया का समाज का तो ये बड़े जुझारू/साबित होते पर इनकी सुध नहीं किसी को ।’ वास्तव में इनकी किसी को सुध न होना ही सबसे बड़ी विडंबना है। शारीरिक श्रम करने वालों के प्रति यह उपेक्षा का भाव सदियों से चला आ रहा है। उनके श्रम की तो सबको जरूरत होती है लेकिन उसे उचित मूल्य और सम्मान विरले ही देते हैं। उनकी स्थिति बदलने की कोई नहीं सोचता है। आज लोकतंत्र में सभी राजनीतिक पार्टियां उसके वोट को तो पाना चाहती हैं,जिसके लिए उसे सब्जबाग भी दिखाए जाते हैं पर चुनाव जीतने के बाद उन्हें सभी भूल जाते हैं।
वीरेन दा का लंबी कविताओं में कहने का जो अंदाज है, वह मुझे निराला लगता है। वह अंदाज कविता में कथा का आनंद तो देता ही है, साथ ही अपने समय और समाज की विसंगति और विडंबनाओं को बहुत बारीकी से उभार देता है। जिस घटना,चरित्र या जीवन-वृत्त पर एक लम्बी कहानी या उपन्यास लिखा जा सकता है, उसे वीरेन डंगवाल एक कविता में बहुत प्रभावशाली ढंग से कह डालते हैं, लगता ही नहीं कि उसमें कुछ छूट रहा है। ऐसा नहीं कि वे अपनी इन कविताओं में दूर की कौड़ी लाकर उसे धो-पोछ और सजा-संवार कर प्रस्तुत करते हों, बल्कि वह कथ्य के भीतर प्रवेश कर उससे एक आत्मीय सम्बन्ध स्थापित कर उसे कविता में बदल देते हैं। इसलिए उनकी कविताओं को पढ़ते हुए पाठक भी उसी भावभूमि में पहुँच जाता है, जहाँ कवि था। उसे इन कविताओं में ‘ग्रीष्म की तेजस्विता’,‘शहद का उष्म ताप’ और उमड़ते बादलों की रगड़ से पैदा मुखर गुस्सा महसूस होता है। कथ्य से आत्मीय सम्बन्ध बना और उसमें गहरे तक प्रवेश कर कविता रचने की उनकी रचना प्रक्रिया को हम विभिन्न शहरों और चरित्रों पर लिखी गई उनकी कविताओं में देख सकते हैं। किसी जगह,व्यक्ति और वस्तु से आत्मीय सम्बन्ध बनाए बिना इतनी मर्मस्पर्शी कविताएं नहीं लिखी जा सकती हैं। साधारण चीजों पर असाधारण कविताएं लिख लेना इतना आसान नहीं होता है। यह आत्मीयता का ही कमाल है। तभी तो हरी मिर्च के बगल और उबले चनों के नाजुक ढेर पर रखा नींबू किसी फूल से बेहतर नजर आता है और पोदीने की ख़ुश्बू अलौकिक लगती है। चौंधा मार रही धूप में कबाड़ी बच्चे की ‘पेप्पोर,रद्दी पेप्पोर!’ की पुकार अवसाद और अकेलेपन से भर देती है। ‘खुशी से गोरूओं का नथुने फुंकारना और कान फटफटाना’ भी दिख जाता है। वह बरेली, सहारनपुर, इलाहाबाद, नैनीताल,कानपुर, मेरठ,दिल्ली आदि शहरों में रहे, इन तमाम शहरों को उन्होंने अपनी कविताओं में बहुत आत्मीय तरीके से याद किया है। कितनी बड़ी बात है कि आप जिस जगह भी जाते हैं और जिन लोगों से मिलते हैं ,उनके साथ अपने गहरे सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं, एक सच्चा कवि ही ऐसा कर सकता है। वही जो पूरी पृथ्वी को प्यार करता है, अपनी ही जगह और नाते-रिश्तेदारों के मोह में नहीं बंधा रहता है। यह सब एक अलग रास्ता पकड़कर ही संभव है। वह रास्ता नहीं जो ‘सीकरी’ को जाता है बल्कि एक ऐसा रास्ता जो उन गली-मुहल्लों,बीहड़ों,रौखड़ों,पहाड़ों और रेगिस्तानों से होकर गुजरता है, जहां फौजी,कश्यप,धीमर,निषाद,मल्लाह,धुनार,शिल्पकार,लुहार,दर्जी,कारीगर,मजूर,कबाड़ी, फेरीवाले रहते हैं। कटरी की रुकुमिनी और उसकी माता के दर्द को इसी रास्ते से चलकर महसूस किया जा सकता है। यह एक ऐसा रास्ता है जिसे साधारण जन तो जानते हैं, लेकिन मर्मज्ञ नहीं। यह बहुत घुमावदार रास्ता है। वीरेन दा जीवनपर्यंत इसी रस्ते पर चलते रहे। हमेशा सत्ता से एक दूरी बनाए रखी और दृढ़ता से इस संकल्प को पूरा किया-‘दिल्ली कहकर हरगिज/कोई तुक न मिलाऊँ/म्याऊँ कभी न बोलूँ।’ इसी संकल्प के चलते वह हमेशा सत्ता के सामने प्रश्न खड़े करते रहे, कभी ‘रामसिंह’ तो कभी स्रश्टा और तारंता बाबू के बहाने- तुम किसकी चौकसी करते हो रामसिंह?/तुम बंदूक के घोड़े पर रखी किसकी ऊँगली हो?/.....कौन हैं वे ,कौन/.....जो बच्चों की नींद में डर की तरह दाखिल होते हैं?/ जो रोज रक्तपात करते हैं और मृतकों के लिए शोकगीत गाते हैं? आगे वीरेन खुद बताते हैं-वे माहिर लोग हैं रामसिंह/वे हत्या को भी कला में बदल देते हैं। हत्या को कैसे कला में बदला जाता है? इस प्रकिया को वीरेन ‘रामसिंह’ कविता में बहुत खूबसूरती से बताते हैं। एक अलग रास्ते पर चलकर ही वह ‘पी.टी.उषा’ की चमकती आँखों में भूख को पहचानने वाली विनम्रता को देख पाए और कह पाए-मत बैठना पी.टी. उषा/इनाम में मिली उस मारुति पर मन में भी इतराते हुए/बल्कि हवाई जहाज में जाओ/तो पैर भी रख लेना गद्दी पर। कवि का ऐसा कहना एक तरह से सभ्यता के नाम पर किए जाने वाले आडंबरों को प्रश्नांकित करना है। वह मानते हैं कि आडबंरों से कोई बड़ा नहीं बनता है,बड़ा तो आदमी अपने उस आचार-व्यवहार से होता है जो उसे साधारण जनों से जोड़ता है। वह साफ-साफ कहते हैं- वे जो जानते हैं बेआवाज जबड़े को सभ्यता/दुनिया के सबसे खतरनाक खाऊ लोग हैं। अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए, पता चल जाता है कि वीरेन दा कितनी गहरी और प्रमाणिक बात कह गए हैं।
एक और बात जो मुझे उनकी कविता में खास लगती है, वह है उनकी कविताओं की ध्वन्यात्मकता और खिलंदड़ापन। ऐसी ध्वन्यात्मकता मुझे उनके समकालीनों में तो कम से कम नहीं ही दिखाई देती है। वह ध्वन्यात्मक बिम्बों के माध्यम से कविता में एक लय तो पैदा करते ही हैं, साथ ही एक अलग तरह का कौतूहल भी। ये ध्वनियां कविता में नए अर्थों का संधान भी करती हैं। बहुत देर तक टन..टन..घन...घन...तड़...तड़....सांय-सांय ...चट...चट...चट.... चिक...चिक...चीं...चीं.....भों-पों-भों .....चर्र-चर्र....गुर्र-गुर्र....की ध्वनियां कान में बजती रहती हैं। वीरेन डंगवाल भाषा में तोड़फोड़ करते हैं। नए-नए शब्दों को जन्म देते हैं। लोकधुनों और लोकगीतों की शैली का भी सुंदर इस्तेमाल करते हैं। उनकी काव्यभाषा और शिल्प में हमें गैर-जरूरी बांकपन नहीं दिखाई देता है। कथ्य ही नहीं बल्कि भाषा में भी वह जन के करीब हैं। भले ही तत्सम शब्दों का उनकी कविताओं में पर्याप्त इस्तेमाल हुआ है, बावजूद उनकी भाषा बोलचाल की भाषा से दूर नहीं गयी है। वह पुरखे कवि नाजिम हिकमत की इस बात के समर्थक थे कि कविता की भाषा और जीवन की भाषा अलग-अलग नहीं होनी चाहिए। इस बात का उन्होंने हमेशा ध्यान भी रखा। वह अपनी बात को कहने के लिए एक नाट्य-निर्देशक की भाँति पहले मंच सजाते हैं, जिसमें पूरा परिवेश जीवंत हो उठता हैं और इस तरह कविता की अंतर्वस्तु अलग से चमक उठती है। उदाहरण के लिए उनकी लम्बी कविता ‘कटरी की रुकुमिनी और उसकी माता की खंडित गद्य कथा’ देखी जा सकती है। इसमें रुकुमिनी की वेदना को व्यक्त करने के लिए पहले कटरी का पूरा सामाजिक और भौगोलिक परिदृश्य बारीकी से चित्रित करते हैं, तब रूकुमिनी को परिचित कराते हैं। शायद यदि ऐसा नहीं किया जाता तो रुकुमिनी और उसकी माता की वेदना उतनी गहराई से पाठक की संवेदना का हिस्सा नहीं बन पाती। न ही एक गरीब स्त्री कम उम्र में ही अपने चीथड़ा होते जीवन और शरीर के माध्यम से अपने समाज के कई जटिल और वीभत्स रहस्य को जानने की प्रक्रिया को इतनी मार्मिक रूप से व्यंजित कर पाती। यही बात हम ‘गंगा स्तवन’ कविता में भी देख सकते हैं। ये दोनों कविताएं स्त्री की पीड़ा और विडम्बना को भी बहुत तीव्रता से उभारती हैं। लगता जैसे कवि ने अपना हृदय उड़ेल कर रख दिया हो। कथ्य से ऐसी अंतरंगता बहुत कम दिखाई देती है। इसी अंतरंगता के चलते कवि एक स्त्री के उपले की तरह सुलगते दिल को देख पाता है और कवि की आँखों में नम बादल उमड़ आते हैं। यह नम बादल कवि की आँखों तक ही नहीं रहते हैं बल्कि पाठकों की आँखों में भी उतर आते हैं। वे उसके उल्लास और यातना दोनों को महसूस कर पाते हैं।
यहाँ स्त्री संदर्भ आया है,इसलिए इस बात का उल्लेख करता चलूँ कि तमाम परेशानियों,अभावों और विडम्बनाओं के बावजूद भी वीरेन दा के स्त्री पात्रों की सपने देखने की आदत का न जाना उनकी कविताओं को एक अलग ऊंचाई प्रदान करता है। उनकी औरतों का यह कहना-‘हम हैं इच्छा मृग/वंचित स्वप्नों की चरागाह में तो/ चैकडि़याँ मार लेने दो हमें कमबख्तो!’ पितृसत्ता के खिलाफ एक युद्धघोष की तरह लगता है। वीरेन औरतों की बेखौफ आजादी के समर्थक रहे हैं और इस बेखौफ आजादी की शुरुआत अपने घर से ही करते हैं। अपनी बिटिया पर लिखी कविता ‘समता के लिए’ में वह कहते हैं-‘एक दिन बड़ी होना/ सब जगह घूमना तू/हमारी इच्छाओं को मजबूत जूतों की तरह पहने/ प्रेम करना निर्बाध/नीचे झाँक कर सूर्य को उगते हुए देखना।’ ऐसे समय में जब प्रेम करने वाले लड़के-लड़कियों को ‘ऑनर किलिंग’ का शिकार होना पड़ रहा हो और प्रेम करना प्रतिशोध का कारण बन गया हो, कवि द्वारा अपनी पुत्री को निर्बाध प्रेम करने की छूट देना साहसिक और ईमानदार पहल कही जा सकती है। यहाँ प्रेम करने की छूट देना केवल प्रेम करने तक सीमित होकर नहीं रह जाता है बल्कि उस सामाजिक ताने-बाने के विरोध में खड़ा होना है जो स्त्री की आजादी को स्वीकार नहीं करता है। स्त्री के लिए उनके मन में कितना सम्मान है इन पंक्तियों से समझा जा सकता है-और स्त्री का शरीर!/तुम जानते नहीं,जब-जब तुम उसे छूते हो/चाहे किसी भाव से/तब उसमें से ले जाते हो तुम/उसकी आत्मा का कोई अंश/जिसके खालीपन में पटकती है वह अपना शरीर।
वीरेन दा की बात कहने का तरीका बड़ा अनूठा है। उनकी एक छोटी सी कविता में भी हमें बहुत अधिक विस्तार दिखाई देता है। वह कविता कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, कह नहीं सकते हैं। जैसे बात साइकिल से शुरू करते हैं पहुंच जाते हैं षहर के रहने के तौर-तरीकों पर ,गली-मुहल्ले के व्यवहार पर, उन दिनों पर जब लोग शहरों में पेड़ों के नीचे ही शरण ले लेते थे। रात के एक बजे भी कहीं से भी एक रिक्शे में अपना साज-सामान लादे आ जाते थे। साइकिल के बहाने अपने पूरे दौर को याद करते हैं। उसकी राजनीति पर बात करते हैं। साइकिल के माध्यम से निम्न-मध्यवर्ग के जीवन और सोच को समाने रख देते हैं। एक ही कविता में इतने सारे आयाम कम ही दिखाई देते हैं। एक की बात करते हुए दूसरे में प्रवेश कर जाना, फिर मूल पर वापस लौट आना उनके काव्य-शिल्प की विशिष्टता है। पता ही नहीं चलता है उनका प्रतीक कब पात्र में बदल गया और पात्र प्रतीक में। जैसे- गंगा नदी की बात करते हुए उसे स्त्री जीवन से जोड़ देना, मक्खियों की बात करते हुए कूड़ा बीनने वालों तक पहुंच जाना। बड़ी बात यह है कि ऐसा करते हुए कविता में कहीं बिखराव या टूटन नजर नहीं आती है। कविता की संश्लिष्टता बनी रहती है। अंतर्वस्तु के विस्तार के चलते कुछ कविताएं पहली बार पढ़ने में समझ में नहीं भी आती हैं। इसके पीछे कारण हैं जिसके लिए उन्हीं की एक कविता को उद्धरित किया जा सकता है-जरा सम्हल कर/धीरज से पढ़/बार-बार पढ़/ठहर-ठहर कर/आँख मूंद कर आँख खोल कर/गल्प नहीं है/कविता है यह।
वीरेन दा की कविताओं में आए बिम्ब,प्रतीक और रूपक इतने ताजे हैं कि उनकी ताजगी बहुत लम्बे समय तक पाठक को तरोताजा किए रहती है। इनकी एक लम्बी सूची तैयार की जा सकती है। बिम्बों और प्रतीकों के टटकेपन की दृष्टि से मुझे उनकी ‘जहाँ मैं हूँ’ कविता बहुत पसंद है, जिसको यहां उल्लखित करने का लोभ में संवरण नहीं कर पा रहा हूँ-जहाँ नशा टूटता है ककड़ी की तरह/जहाँ रात अपनी सबसे डरावना बैंड बजाती है/सबसे मद्धिम सुरों में/एक स्त्री जहाँ करती है प्रेम का सुदूर इशारा/जहाँ मछली का ताजा पंजर चबाता है ऊदबिलाव/जहाँ भ्रष्टाचार का सौंदर्यशास्त्र रचते हैं/नीच शासक/जहाँ कोई विधवा अकेले में रोती है चुपचाप/चौतरफा बोझ है संसार/जहाँ कौड़ा तापते अब भी अडिग साथी/मशगूल हैं किले को भेदने की/नयी तरकीब खोजने में। नशे का ककड़ी की तरह टूटना, रात का बैंड बजाना, मछली का ताजा पंजर चबाता ऊदबिलाव जैसे बिंब शायद ही आपको कहीं पढ़ने को मिले हों। ऐसे अनेक उदाहरण हैं उनकी कविताओं में, जहां बिंब-प्रतीक और रूपक अनायास अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फिर दूर नहीं जाने देते हैं। पाठक उन्हीं के साथ घूमता रहता है। बुरी खबर लेकर आने वाले पोस्टकार्ड के लिए उनका यह बिंब देखिए-तब उनकी सूरत होती है/कान-पूंछ दबाए घरेलू कुत्ते की तरह/जो कर आया हो कोई निखिद्द काम..... इसी तरह नींद का एक चित्र आता है उनके यहां-मुझे तो वह नींद सबसे पसंद है/जो एक अजीब हल्के-गरू उतार में/धप से उतरती है/पेड़ से सूखकर गिरते आकस्मिक नारियल की तरह/एक निर्जन में।.....बादलों भरी द्वाभा है भादों की शाम की/फेफड़ों में पिपरमिंट सी शीतल हवा का स्वाद...........शरद की है धूप/कुछ सीली जरा सी गर्म/वे लगे शिशु फूल गोभी के/नगीने से जगमाते....माता थी/कुएं की फूटी जगत पर डगमगाता इकहरा पीपल.....अकेलापन शाम का तारा था/इकलौता /जिसे मैंने गटका /नींद की गोली की तरह/मगर मैं सोया नहीं।.. गजब की कल्पनाशीलता और इंद्रियबोध के दर्शन होते हैं इन बिंबों में। इनसे पता चलता था कि यह कवि जीवन के कितने निकट था। जीवनराग से लबालब भरा हुआ।
वीरेन दा मरते दम तक अपने समय और समाज के बारे में बहुत कुछ कहते रहे। हमें अपने समय की क्रूरताओं के प्रति सचेत करते रहे । ‘इसी दुनिया में’ , ‘दुश्चक्र में स्रष्टा’ और ‘स्याही ताल ’ नाम से तीन कविता संग्रह हमें दे गए। कैंसर जैसे पीड़ादायी रोग से लड़ते हुए भी अपनी बात कहते रहे बावजूद इसके उनको यह लगता रहा कि अभी बहुत कुछ है जो कहना बाकी है - ‘अनिद्रा की रेत पर तड़-पड़ तड़पती रात/रह गई है रह गई है अभी कहने से/सबसे जरूरी बात।’ अधूरेपन का यह अहसास एक बड़े और सच्चे कवि को ही हो सकता है अन्यथा हमारे दौर में तो ऐसे भी बहुत सारे कवि हैं जो चार कविता लिखने के बात खुद को महाकवि समझने लगते हैं। इतनी आत्ममुग्धता से ग्रस्त हो जाते हैं कि उनको अपनी कविता के अलावा कहीं कुछ नजर ही नहीं आता है। वीरेन दा को न अपने कवि होने पर और न अपनी कविता पर कोई गुमान या अहंकार था। उन्हें न कविता सुनाने और न छपाने का कभी कोई मोह रहा। न उन्होंने महज कवि बने रहने के लिए और संपादकों की मांग पर कोई कविता लिखी। उनके लिए ‘कविता आदमी के भीतर से निकली एक गहरी पुकार है’।(पाब्लो नेरुदा) ऐसी पुकार जो प्रकाश की व्याख्या करती रही। वह तो हमेशा बिल्कुल सहज-सरल बने रहे। सरलता उनके लिए एक जीवन-मूल्य था। तभी तो वह इतनी विनम्रता से कह पाए-एक कवि और कर ही क्या सकता है/सही बने रहने की कोशिश के सिवा।’ इस सही बने रहने की कोशिश में वीरेन दा की लालसा थी-यह जो सर्वव्यापी हत्या का कुचक्र/चलता दिखाई देता है भुवन- मंडल में मुनाफे के लिए/मनुष्य की आत्मा को रौंद डालने वाला/रचा जाता है यह जो घमासाम /ब्लू फिल्मों,वालमार्टों,हथियारों,धर्मों/और विचारों के माध्यम से/उकसाने वाला युद्धों/बलात्कारों और व्याभिचार के लिए/ अहर्निष चलते इस महासंग्राम में/हे महाजीवन चल सकूं कम से कम/एक कदम तेरे साथ/प्रेम के लिए /शांति के लिए। इस उद्देश्य से पूरी दुनिया को एक एस एम एस लिख भेजना चाहते हैं- ‘भूख और अत्याचार का अंत हो/घृणा का नाश हो /रहो सच्चे प्यार रहो
सबके हृदयों में/दुर्लभ मासूमियत बन कर।’ अद्भुत ‘दुर्लभ मासूमियत’ से भरा यह कवि हमेशा ‘हजार जुल्मों से सताए लोगों’ के साथ खड़ा रहा। अपने को उसका एक हिस्सा मानता रहा। उनकी आवाज को बुलंद करता रहा। उन साथियों के साथ रहा जो किला भेदने की नयी तरकीब हासिल करने में लगे रहे। उन्हें अपना स्नेह,ममता और प्यार दिया। चालाकी से हमेशा दूर रहा। अपने जन के दुःख-दर्द को महसूस करता रहा। अपनी जमीन से गहराई तक जुड़ा रहा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वे वृक्ष ढह जाते हैं जिनकी जड़ें जमीन की सिर्फ पपड़ी में होती हैं। कठोर दिनों का सामना करने और जीवन का सत पाने के लिए अपनी जमीन से जुड़ना कवि को आवश्यक लगा-अभी तो झेलना होगा बहुत कुछ/आगे दिन सख़त हैं/पहुँचना होगा अपनी जड़ों के रोम-कूपों को/धरा की तलहटी तक/हाँ जी ,बहुत पानी है वहाँ अब भी/समुद्रों की खोयी हुई याद/खींच लाना होगा वहीं से सत जीवन का/ तभी होगा खड़ा रहना । अपनी जमीन पर दृढ़ता से खड़े होकर ही सूखते जाते प्रेम के स्रोतों को फिर से हरा किया जा सकता है, और भीषण अंधे कोलाहल कलरव से भरी रात से मुक्ति पाई जा सकती है।