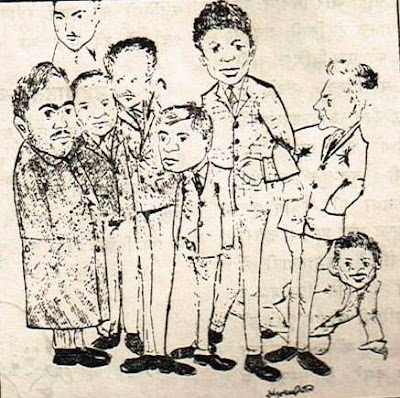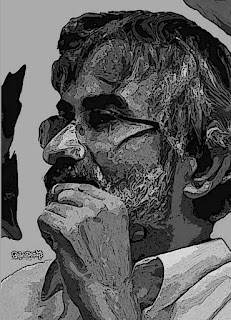महाभूत चन्दन राय ने कविता में एक कठिन राह पकड़ी है। सरलीकरणों के बरअक्स वे एक जटिल लग सकने वाला संसार रच रहे हैं। उनके लिखे में ख़ूब अभिधा है। वे संवाद में यक़ीन रखने वाले कवि हैं। कोई संवाद उतना जटिल होता नहीं, जितना एकबारगी लग सकता है। इन कविताओं का गद्य कठोर है। कविता, कविता होने से पहले एक बयान है - इस बिसरी हुई याद को वे अचानक केन्द्र में ले लाए हैं। कविता में चहुंओर चल रहे बखानों के विरुद्ध ये तीखे और बेधक बयान एक कहीं अधिक मार्मिक कार्रवाई है। इनका सम्बोधन किसी ओजस्वी भाषण का-सा है। समकालीन सत्ता की राजनीति और साहित्य की राजनीति से खुली भिड़न्त आज के इस कवि के सामर्थ्य का पता देती है, क्योंकि ठीक वहीं कविता और जाहिर सफलताओं से चूक जाने का ख़तरा भी माजूद है। कितने कवि हैं जो ख़तरे के बीच इस तरह चले जाने को ही अपने शिल्प बना लेना चाहेंगे?
मेरा छटपटाता हृदय इन कविताओं के बीच से गुज़रते और भी छटपटाता है। कला के धुंधलकों में छुप गए कितने ही सूर्य हमारे, तब उस लुका-छुपी के बीच इन कविताओं की साफ लाल लपट मुझे आश्वस्त करती है। आगे इस आग की ज़रूरत होगी हमें। इस आग में उतरता हूं तो 'चकमक की चिंगारियां'याद आती है –
अधूरी और सतही जिन्दगी के गर्म रास्तों पर
हमारा गुप्त मन
निज में सिकुड़ता जा रहा
जैसे कि हब्शी एक गहरा स्याह
गोरों की निगाह से अलग ओझल
सिमटकर सिफ़र होना चाहता हो जल्द
मानों क़ीमती मजमून
गहरी,ग़ैर-क़ानूनी किताबों,ज़ब्त पत्रों का
(मुक्तिबोध)
***
हवाकेरुखकेविरुद्ध
( 1 )
यह कैसी बर्बर हवा बह रही है..
की कविताओं में समय-दर्ज यथार्थ के सारे हर्फ़ उड़ गए है..
कलमें तानाशाहों की रंगशालाओं में फाँसी झूल रही है
सच झूठ के पांवों में दासों सा हाथ जोड़े पड़ा है
और शैतानों को दिहाड़ी बजा रहे हैं इस सदी के देवता-गण
जो सबसे झूठे दगाबाज और मक्कार थे...
वो सिहांसनों पर विराजित दे रहे हैं न्याय के आदेश !
( २)
मैं शहर के बीचो-बीच खड़ा पड़ताल करने की कोशिश करता हूँ
यह कैसी निर्लज्ज हवा बह रही है की समय इतना लफंगा हो गया है
की दुर्घटनाओं का रत्ती भर भी शोक नहीं मानता
संवेदना लो बॉटम जींस डाले हर्ट-लैस अर्द्धनग्न घूम रही है
निजता निजीकरण में और उदारता उदारीकरण के बाजार में तब्दील हो चुकी है
धर्म-जाति-भाषा-शब्द-रोटी और देह सब कुछ बिक रहा है खुलेआम
( 3 )
मैं पड़ताल करता हूँ क्या है इस बर्बर हवा का रुख..
की जिसमे धर्मनिरपेक्षताकीहरबातमस्जिद की गुंबदसेशुरूहोतीहै
और मंदिरों की दीवारों पर आकरखत्महोतीहै
यहकैसी विषाक्तहवाबहरहीहैकी
कोईभीऐरा-गैरानत्थूखेरादिनदहाड़े लिख देता है
धर्मकीदीवार पर..
"राम-रहीम जानी-दुश्मन"
औरलोगएकदूसरेकागलारेतनेलगतेहैं!
( 4 )
मैं जानना चाहता हूँ इस हवा का रुख ...
जिसमे मैं और आप दोनों बड़ी बेफिक्री से सांस लेते हैं
की अयोध्या की बाबरी मस्जिद में दाखिल होते हुए
उसने अल्लाह को वजूहात का हक अदा किया था या नहीं
और राम लला के खंडित परिसर में भीतर प्रवेश करने से पहले
उसने अपने इस्लामी पाँव पखारे थे या नहीं…?
वह किस-किस जगह कितनी-कितनी हिन्दू थी और कितनी-कितनी मुसलमान..?
मंदिर-मस्जिद की विवादित जमीन पर उसका रुख क्या है ?
इस हवा में सांस लेने के लिए मेरा यह जान लेना बेहद आवश्यक है
वह झोपड़ियों में कितनी खिन्न थी और महलों में थी कितनी प्रसन्न !
( 5 )
यह कैसी हवा बह रही है की जिसमे हम अपने-अपने मुँह छुपाये
अपनी-अपनी मजबूरियों और समझौतों के साथ घर में नजरबंद हैं ..
हमारी वैचारिकता सम्मोहन-ग्रस्त मूढ़ हामी लिए अपने सर झुकाये
भेड़ों सी भेड़-झुंडों में चली जा रही है
मसलन हम समूहों में बोलते है और समूहों में करते है इंकार
अब एक समूह तय करता है हमारी बौद्धिकता ,हमारे विरोध
हमारी आवाज हमारी प्रतिबद्धता हमारा रुख एक समूह का रुख हैं
ये कैसी हवा बह रही है की जिसके साथ हम कोरेकागजों से उड़े जाते हैं
और हमारे पास अपने नुकीलेइंकार तक नहीं हैं!
( 6 )
मैं देख रहा हूँ इसी बर्बर हवा में कुछ जीवित वस्तुओं का रुख ..
एक बाँस अभी भी तना हुआ अकड़ रहा है हवा के विमुख
एक अमरबेल रस्सियों के सहारे झूल रही है ,
अच्छे दिनों की परिकल्पना के दिवास्वप्नों में डूबा एक अर्धमृत रीढ़-हीन देश
ऑंखें भींचे एक मायावी के पीछे चला जा रहा है
हिटलर का पुनर्जन्म हो रहा है
और सद्दाम जैसे धीरे-धीरे इस समय में लौट रहा है !
( 7 )
मैं देख रहा हूँ इस विचारशून्य समय में
जब समूची विपक्षता हवा के रुख की तरफ रुख कर चली जा रही है
इस समय में जब चीजें इतनी मृतप्राय और निर्जीव हो गयी हैं
एक हरी दूब मुस्कराती हुई पूरे साहस के साथ खड़ी है
हवा के इस रुख के विरुद्ध !
***
जीवितहोनेकामहत्व
महत्वइसबातकानही..
कीवहलड़ाऔरमारागया
महत्वइसबातकाहैकी
यहजानतेहुएभीकीवहमारदियाजाएगा
वह लड़ा!
सम्भवतःइसबातकाकोईअर्थनहोकी
वहज़बप्रतिरोधकेगलगलेकररहाथा
उसकीआवाजकेप्रहारनेकहींकोईहलचलपैदानहीकी
कहींविरोधकीकोईश्रृंखलानहीफूटी
कोईकिलानहीढहाकोईदिवारकहींनहीगिरी
परइसबातकाअर्थसदैवजीवितरहेगाकी
जबचारोंतरफ़पसराहुआथामुर्दासन्नाटा
वहपागलोंकीतरहबोलरहाथा !
जबसहमतियाँसामूहिकताकीगलबहियाँडाले
बेशर्मोंकीतरहघूमरहीथी
औरहवाकारुखतयकररहीथी
पक्षधरताकीवस्तुस्थिति
वहअकेलाहीहवाकेरुखकेविरुद्ध
खड़ाहस्तक्षेपकररहाथा !
जबलोगअपनेहोनेकेअभिप्रायसेभागरहेथे
वहअपनेहोनेकेमतलबकेसाथअड़ाखड़ाथा
औरअसम्भवकोसम्भवबनानेकीअपनीजिदमें
बचाएहुआथाप्रतिनिषेधकीभूमिका
जबहरचीजबिकाऊऔरमृतप्रायःहोचलीथी
वहबचायेहुएथाजीवितहोनेकामहत्व..
औरइसबातकेमायनेकभीमृतनहीहोंगे !
***
मेडइनइंडिया
अबमैंभूखसेनहीमरूँगा..
नहींमरूंगाडेंगू मलेरियायाचिकनगुनियासे
अ-विकासकामच्छरमुझेनहींमारेगा डंक
मेरेफेफड़ोंमेंनहींरेंगेगेटी.बी. केकीड़े
मेरीआँतोंमेंबिलबिलातेगरीबीकेचूहे
अब फाड़ेंगे नहींमेरापेट
गरीबीमेरेलिएमहजएकअफवाहहै
पानीकीजगहपियूँगादारु
खाऊंगाडॉलरयूरोऔरपाउंड
बेचूंगानींदके घोड़े !
मैंअबपृथ्वीपरनहीमरूँगा..
कीड़ेमकौड़ोंकीसीमौत !!
अबतो चीनसेदनदनातीआएगीकोईचाइनापिस्तौल
कोईअमरीकीस्मार्टसिटीमेरेमुहल्लेमेंआबसेगी
रूससेउड़ताआएगाकोईयुद्धविमान
जापानसेदौड़तीआएगीकोईजापानीरेल
जर्मनीसेआयातहोंगेहिटलर
हवामेंउड़तेहोंगेशॉपिंगमाल
बरसतीहोगीआसमानसेइंग्लिशवाइन !
मैंअबकभीमंगलयानमेंबैठा
कभीचंद्र-यानमें बैठा
कभीप्लूटोपर...
कभीजूपिटरपर ..
कभीवीनसपर..
नरककेमसीहाओंसे
"मृत्युपरचर्चा"करूंगाऔरबेचूंगा"मौत"
कहूँगामहोदय.. कममेकइनइण्डिया
जीवनयहाँमहंगाहैतोक्यामौतयहाँपरसस्तीहै
आखिरग्लोबलाइजेशनकाजमानाहैसाहब !
फिरकोईचन्द्रमाहीक्योंनमुझपरगिरपड़े
मैंमंगलकेमलबेकेनीचेहीक्योंन दबमरूं
डूबजाऊंचाहेकिसीहिन्दमहासागरमें
फिरकोईउल्काहीमुझपरटूट पड़े
फिरकोईताबूतहो. चिताहोयाकब्र .
मुझेफूंकों ,दफनाओं, जिन्दाजलादो
मिलहीजानाहैयमलोकमें ..
"आनअराइवलवीजा"
मैंकिसीभीविदेशनितिकेतहतमरूँ...
मरूंगाआखिरकर"पूंजीवादी"मौत
फिरमैंनेकराभीतोलियाहै ..
मरनेकेबाद ...
आदमीकोअमीरकरदेनेवालाबीमा !
***
अमानुषोंकेप्रति
मैंमहजअफवाहहूँ...
तुमसनसनीखेजखबरहो !
मैंभूखेकीथालीकाग्रहणहूँ
तुमगलेतकमदिराकीतरावटहो !
मैंटूटीझोपडीहूँ
तुमसोनेकामहलहो !
मैंजनताकीजूतीहूँ
तुमराजाकापाँवहो !
मैंमेहनतकीगन्धहूँ..
तुमविलासकाइत्रहो !
मैंआपरेशनकीटेबुलपरबिकनेवाली
किडनीहूँ ,आंतहूँ , आँखहूँ...
तुमसाइनकियाब्लैंकचैकहो !
मैंकोठेपरबिकनेवालासामानहूँ..
कारीगरकेकटनेवालाहाथहूँ
तुममालदारखरीदारहो
धारदारऔजारहो !
मतमानो..
मेरेपासकलेजाहै
मुर्गाहूँ
खामोशतुम्हारेगंडासेकेनीचेकटजाऊँगा !
तुम्हारेनथुनोंमेंघुसरहीहैजोहवा
उसेसुंघों...
येकिसकेलहूकीगन्धहै ?
गरकानखराबनहो
तोकानोंकेपासझाँखभरगयीहवामेंसुनो
येकिसकेकत्लकीचीखहै ?
मेरेशब्दोंमेंउसीकत्लकीबूहै
मुझेहरवक्तदिखायीपड़तीहैवोस्त्री
जो"बचाओबचाओ"चीखरहीहै !
क्यातुम्हेभीकुछमहसूसहोताहैऐसा
गरअमानुषहीहो.
तोफिरक्याकहूँ ??
***
मतमतमत
मतदेखोआईनाही...
की वह तो तुम्हारा रूप ही बघारता है
फिर वह दोष भी दिखाएगा
तो तुम कहाँ देखोगे ?
मतजाओकिसीपोएट्रीफेस्टिवलमें
शिमला,चिमला, चकादमीयापानपीठ
बजाओ बंशीधर बंशी अकेले ही अकेले
पुरस्कारों की मुंह दिखाई से दूर
कुंवारे ही बने रहो ...
रहो अलग थलग किसी से मत मिलो !
मतपूजोउनकेपाँव..
जिनके सर बहुत ऊँचे हो
जिनकी आँखे झुकती ही नही
और जिनकी गर्दनों में अकड़न हो !
खूब जियो नास्तिकता का दुस्साहस
गढ़ो सहारे की आदत के विरुद्ध जीने की पद्धति
मतमानोजिसेअबतकबदलानहीगया..
उसे बदला नही जा सकता
मत मानो उसे जिसे राजदरबारों की प्रथा में
मानना बेहद जरूरी है
खूब कहो जैसे कहते हो, कहते रहे हो
चीखकर, धीमे से, लिखकर, गाकर,बड़बड़ाकर
करो इंकार जितना कर सकते हो !
मतखोलनाअपनेमनकेद्वार..
पर इतना भर खुले रहना
की अपने बनाये सिद्धांतों के भीतर
कहीं तुम ही कैद होकर दम न तोड़ दो
इच्छा करना पर लोभ मत करना
गलतियाँ करना पर अपराध मत करना
गर्व करना पर अभिमान मत करना
विरुद्ध होना पर खिलाफ मत होना
बोलना पर थूकना मत!
बेशक उकताए रहना
अपनी मत मत की मत मत में
पर मत चूकना यह जांचने में भी की
तुम्हारी यह मत मत मत कहीं
तुम्हारा दृष्टिदोष, वाक् दोष या श्रवण दोष न हो
इस"मत मत मत"की दुनिया बनाते हुए
तुम जो मान रहे गढ़ रहे हो रच रहे हो
वह "मत मत मत"इस लगातार कठिन होती दुनिया को
को"सरल"बनाने की कोशिश हो
और यह भी की इस मत मत की मत मत में
तुम कहाँ स्थितहो??
***
बधाई औरपुरस्कार
यह जानते हुएभी मैं लिखता हूँ यथार्थपरक कविताएँ
की महज एक गर्मजोश बधाई भर रह कर दम तोड़ देगा
मेरी लिखी कविताओ का औचित्य और महत्व
तथापि मैं अपनी कविताओं संग पूरे साहस के साथ
इस निर्लज्ज समय से मुठभेड़ करता हूँ !
यह ज्ञात होते हुए भी
की कविता की आवश्यक उपस्थिति
एक पुरस्कार की नियति भर बन कर रह जायेगी
साहित्यिक परिचर्चाएं होगी महज कवि की
कलात्मक सरंचना-गुण-दोष-भाव पर…
मैं निष्प्रभावित यथोचित मनन कर लिखता हूँ
हस्तक्षेपों से भरी कविता…
मैं भयभीत हूँ की
मुझे एक लोकप्रिय कवि की तरह मिल जाएगी
सामाजिक और साहित्यिक स्वीकार्यता
किन्तु जिरह और बहसों के सामाजिक खांचे में
छूटा रहेगा वो रिक्त स्थान
जहाँ बेहद जरुरी था रचने की अनिवार्यता का हस्तक्षेप
कविता महज मनोरंजन की कला नहीं है
कविता नयी संभावनाओं नयी उम्मीदों नए सपने जगाने की भी कला है
अत: कविता लिखने की दुविधा और चिंता से त्रस्त
मैं समाज में कविता की भूमिका और उसकी अनिश्चित स्थिति सेखिन्न
बधाईयों और पुरस्कारों से भयभीत हूँ !
कहीं रचे का यथार्थ और उसकी अनिवार्यता
बधाईयों और पुरस्कारों के मलबे के नीचे दब कर
दम न तोड़ दे
कवियों बधाईयों और पुरस्कारों से सावधान… !
***
थूकना
वह थूकने के कौशल में पूर्णत सक्षम एक थूकबाज था
वह जो भाषा को पीकदान बना देने की हद तक आमादा था
एक दिन उसने अपनी लफंगी शैली में भाषा के भीतर
शब्दों की शक्ल में थूका…
थूकने को आसक्त हो चले एक तथाकथित समुदाय ने
घोषित किया उसे एक प्रतिभाशाली भाषाविद !
इस तरह उस थूकवीर ने जारी रखा अपना थूकने का उपक्रम
धीरे-धीरे उसने अपने समकालीन कवियों कथाकारों
उपन्यासकारों पुरस्कारों पर थूकना शुरू किया
इस दफे थूकने में पारंगत कुछ मूर्धन्य महाशयों ने घोषित किया
उसे नयी पीढ़ी का संभावनाशील आलोचक
बताया गया उसने विकसित की है आलोचना की नई कला !
इस तरह बढ़ता गया उस थूकवीर के थूकने का दुस्साहस
उसने हर घोटी बड़ी घटनाओं व्यवस्थाओं राजनेताओं समाजसेवकों पर थूका
उसने अपने प्रिय अनुजों अप्रिय शत्रुओं और आदरणीय अग्रजों पर समानुपात में थूका
इस दफे कुछ शोहदों ने उसे सार्वजनिक रूप में घोषित किया
उसे अपने हृदयों का नया सम्राट…
प्रतिभाशाली निर्भीक और जोखिमदार !
जबकि थूकना और आलोचना दो अलग-अलग क्रिया है
तथापि धीरे-धीरे लोग उसके साथ मिलकर थूकने लगे..
एक बड़ा जन समूह उसके पदचिह्नों पर चलने लगा..
अन्तत: एक दिन थूकने की नई संस्कृति विकसित करने पर
वह थूकवीर भी हुआ पुरस्कृत
अतएव उससे अपने विचार साझा करने के लिए कहा गया..
किन्तु मंच पर माइक सँभालते ही जो उसने थूकना शुरू किया
तो उसका थूकना रुका ही नहीं…
उसे थूकने की बिमारी थी!
***
आलोचककीआलोचना
यह इस युग के आलोचकों की..
"अहमधर्मिता है या हठधर्मिता"
की अपनी मानक आलोचना के
बाड़ों और अखाड़ों से बाहर कूदते ही
उसकी सारी विद्वता लंगड़ी और गूंगी हो जाती है !
उनकी सारी समकालीनता नव्य की खोज से विमुख
उपेक्षाओं की उस प्राचीन प्राचीर पर बैठी बगुले की वो आँख है
जो अपनी पीठ घुमाए कुछ स्थायी पात्रों की बगुला-भक्तिकररहीहै
उनका सारा ज्ञान अपने ही बनाये बूढ़े प्रतिमानों का वह अशिक्षित है
जिसके बाहर झाँकते ही उसकी दूरदर्शिता खो बैठती है अपनी आँखें..
और महज पढ़ पाती है चिंदी भर निकटता !
जबकि त्रुटियाँ नई संभावनाएं हैं और पूर्णता है समापन..
उसका सारा साहित्यिक-बोध महज पुरस्कृत श्रेष्ठता का
पिछलग्गू हो कर रह गया है
समालोचना अब महज रचनाकार उन्मुखी भाड़े की
प्रशंसा-प्रपत्र होकर रह गयी है
साहित्य की विकास यात्रा पर निकला नव्य का खोजी
वह समन्वेषक रचना से विकेन्द्रित हो खो बैठा है
आलोचना में निहित धैर्य और सन्देहकामुलभूत स्वाभाविक गुण
और अधीर हुए नाचता है कभी यहाँ कभी वहाँ
जैसे चालाक लोमड़ी और खट्टे अंगूर..
जबकि आलोचना है कौए की प्यास
जैसे विदुर की नीति !
समालोचना खो रही है अपना प्राकृतिक सौंदर्य
सूख रहा है आलोचना का हरियर वृक्ष
आलोचक की आलोचना का सुगठित समालोचक प्रयास
ही बचा सकती है अब समालोचना की कस्तूरी सुगंध
और यह एक कवि की आलोचक चिंतित समालोचना है!
***